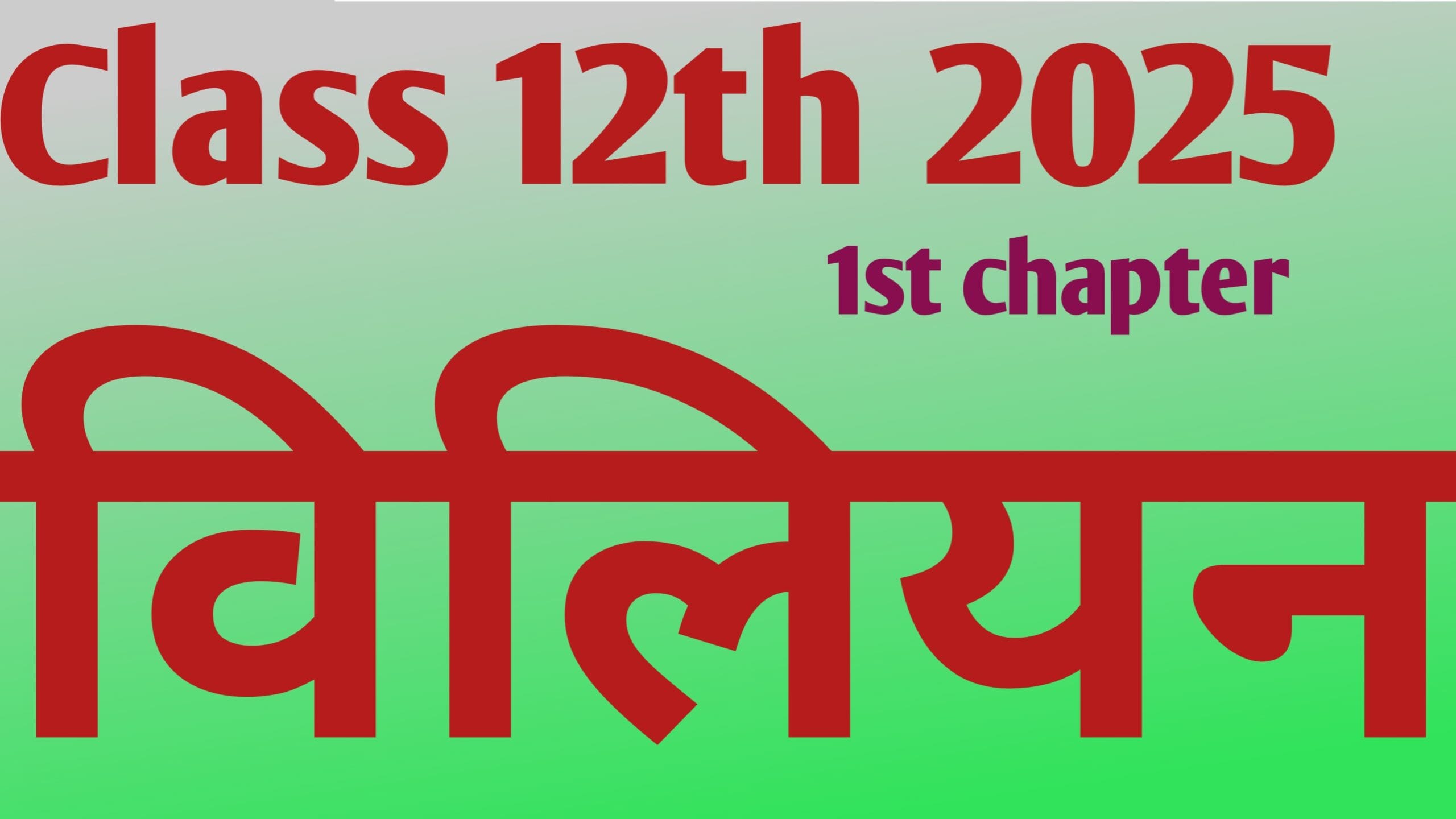हेनरी का नियम (Henry’s Law) – नोट्स
हेनरी का नियम (Henry’s Law) गैसों के विलयन से संबंधित एक महत्वपूर्ण रसायनिक नियम है, जो बताता है कि एक गैस का द्रव में घुलनशीलता (solubility) उसके partial pressure (आंशिक दबाव) के समानुपाती होती है। इस नियम को 1803 में इंग्लैंड के रसायनज्ञ विलियम हेनरी ने प्रस्तुत किया था।
हेनरी का नियम का कथन:
“किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता (संगतता) उसके उस द्रव में गैस के आंशिक दबाव के समानुपाती होती है।”
गैस की घुलनशीलता को “C” और गैस के आंशिक दबाव को “P” माना जाता है, तो हेनरी का नियम निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त किया जाता है: C=kH×PC = k_H \times P
यहाँ,
- C = गैस की घुलनशीलता (mol/L)
- P = गैस का आंशिक दबाव (atm)
- k_H = हेनरी का स्थिरांक (Henry’s law constant), जो उस विशेष गैस और द्रव के लिए विशिष्ट होता है और तापमान पर निर्भर करता है।
हेनरी का नियम समझाने के लिए उदाहरण:
- सोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड (Soda with CO₂ gas):
- जब आप एक सोडा बॉटल खोलते हैं, तो उस बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आंशिक दबाव अधिक होता है। जैसे-जैसे आप बॉटल खोलते हैं और दबाव कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव से बाहर निकलने लगती है। यह हेनरी के नियम का उदाहरण है।
- वायुमंडलीय गैसों का पानी में घुलना:
- जल में घुलने वाली वायुमंडलीय गैसों की मात्रा उनके आंशिक दबाव के समानुपाती होती है। जैसे-जैसे वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है, पानी में अधिक गैस घुलती है।
हेनरी के नियम के महत्वपूर्ण पहलू:
- तापमान का प्रभाव:
- हेनरी का स्थिरांक (k_H) तापमान पर निर्भर करता है। सामान्यतः जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, गैस की घुलनशीलता घटती है।
- उच्च तापमान पर, गैसें अधिकतर द्रव से बाहर निकलने की प्रवृत्ति दिखाती हैं।
- गैस का प्रकार:
- विभिन्न गैसों की घुलनशीलता विभिन्न होती है। हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन (H₂) और ऑक्सीजन (O₂) पानी में अपेक्षाकृत कम घुलती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) और अमोनिया (NH₃) जैसी गैसें अधिक घुलनशील होती हैं।
- द्रव का प्रकार:
- हेनरी का नियम द्रव के प्रकार पर भी निर्भर करता है। यदि द्रव में कोई विशेष पदार्थ हो जो गैस के साथ प्रतिक्रिया करता हो, तो गैस की घुलनशीलता बढ़ सकती है, जैसे अमोनिया (NH₃) और जल में प्रतिक्रिया।
हेनरी का स्थिरांक (Henry’s Law Constant, k_H):
हेनरी का स्थिरांक (k_H) गैस और द्रव के प्रकार के आधार पर भिन्न होता है और यह तापमान पर निर्भर करता है। यदि दो गैसों के लिए समान परिस्थितियाँ हैं, तो उनके लिए हेनरी के स्थिरांक में अंतर होगा।
- उदाहरण: कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का हेनरी स्थिरांक पानी में अन्य गैसों की तुलना में अधिक होता है, जिससे यह अधिक घुलनशील होता है।
हेनरी के नियम का प्रयोग:
- जलवायु अध्ययन:
- समुद्रों में घुलने वाली गैसों का अध्ययन करते समय हेनरी का नियम महत्वपूर्ण होता है। यह समझने में मदद करता है कि समुद्र में कितनी मात्रा में गैसें घुल सकती हैं, जैसे ऑक्सीजन (O₂) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)।
- प्राकृतिक गैसों का परिवहन:
- प्राकृतिक गैसों को लिक्विड रूप में परिवहन करते समय हेनरी के नियम का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि गैसें कितनी मात्रा में द्रवों में घुल सकती हैं।
- वायु प्रदूषण और जल में घुलने वाली गैसों का अध्ययन:
- हेनरी का नियम वायु प्रदूषण नियंत्रण और जलाशयों में घुलने वाली गैसों (जैसे SO₂ और NO₂) के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
हेनरी के नियम के सिद्धांत से संबंधित कुछ सामान्य सवाल:
- किसी गैस की घुलनशीलता और उसके आंशिक दबाव के बीच किस प्रकार का संबंध है?
- गैस की घुलनशीलता उसके आंशिक दबाव के समानुपाती होती है। (Henry’s Law)
- तापमान बढ़ने पर गैस की घुलनशीलता में क्या परिवर्तन होता है?
- तापमान बढ़ने से गैस की घुलनशीलता घट जाती है।
- हेनरी का स्थिरांक (k_H) किस पर निर्भर करता है?
- हेनरी का स्थिरांक गैस और द्रव के प्रकार के साथ-साथ तापमान पर निर्भर करता है।
निष्कर्ष:
हेनरी का नियम गैसों के विलयन की समझ को सरल बनाता है और यह रासायनिक उद्योगों, प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन अध्ययन और जैव रसायन जैसे क्षेत्रों में बहुत उपयोगी होता है।
मोलरता (Molarity) – महत्वपूर्ण नोट्स
मोलरता (Molarity) एक प्रमुख सांद्रता की इकाई है, जिसका उपयोग रासायनिक विलयन के सांद्रता (concentration) को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मोलरता यह बताती है कि किसी घोल में प्रति लीटर घोल में कितने मोल सॉल्यूट (साधारण पदार्थ) उपस्थित हैं।
मोलरता का परिभाषा:
मोलरता (Molarity) को M से व्यक्त किया जाता है और इसे निम्नलिखित सूत्र से परिभाषित किया जाता है: Molarity (M)=मोल सॉल्यूट (moles of solute)घोल का आयतन (volume of solution in liters)\text{Molarity (M)} = \frac{\text{मोल सॉल्यूट (moles of solute)}}{\text{घोल का आयतन (volume of solution in liters)}}
यहाँ,
- मोल सॉल्यूट (moles of solute): यह उस पदार्थ की मोल्स की संख्या है जो घोल में घुला हुआ है।
- घोल का आयतन (volume of solution): यह घोल के कुल आयतन का माप है, जो लीटर में होता है।
मोलरता (M) का मात्रक:
मोलरता (M) का मात्रक मोल/लीटर (mol/L) होता है, जिसे आमतौर पर M के रूप में व्यक्त किया जाता है।
मोलरता का उदाहरण:
- यदि 1 लीटर पानी में 1 मोल NaCl घुलता है, तो इस घोल की मोलरता 1 M (1 मोल प्रति लीटर) होगी।
- यदि 0.5 लीटर पानी में 1 मोल NaCl घुलता है, तो मोलरता होगी: M=1 मोल0.5 लीटर=2 MM = \frac{1 \, \text{मोल}}{0.5 \, \text{लीटर}} = 2 \, \text{M}
मोलरता की गणना:
मोलरता का सूत्र: M=nVM = \frac{n}{V}
जहाँ:
- M = मोलरता (moles of solute per liter of solution)
- n = सॉल्यूट के मोल्स की संख्या
- V = घोल का आयतन (लीटर में)
मोलरता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी:
- मोलरता और आयतन का संबंध:
- यदि घोल का आयतन बढ़ाया जाता है, तो मोलरता घटेगी।
- यदि घोल का आयतन घटाया जाता है, तो मोलरता बढ़ेगी।
- मोलरता और तापमान:
- तापमान में परिवर्तन से घोल का आयतन बदल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मोलरता में भी बदलाव हो सकता है।
- उच्च तापमान पर आयतन बढ़ सकता है, जिससे मोलरता घट सकती है।
- मोलरता और प्रतिक्रिया की गति:
- रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति मोलरता पर निर्भर करती है। उच्च मोलरता वाले घोल में रासायनिक प्रतिक्रिया तेजी से हो सकती है।
मोलरता से संबंधित उदाहरण:
- ध्रुवीय घोल:
- NaCl का 1 M घोल में 1 मोल NaCl प्रति लीटर पानी होगा।
- इसी प्रकार, यदि 1 मोल NaCl को 500 मिलीलीटर पानी में घोला जाए, तो मोलरता होगी: M=1 मोल0.5 लीटर=2 MM = \frac{1 \, \text{मोल}}{0.5 \, \text{लीटर}} = 2 \, \text{M}
- द्रवों के घोल:
- यदि 58.5 ग्राम NaCl (1 मोल) 1 लीटर पानी में घोलें, तो घोल की मोलरता 1 M होगी।
मोलरता से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र:
- मोलरता और मोल की संख्या के बीच संबंध: n=M×Vn = M \times V जहाँ:
- n = सॉल्यूट के मोल्स की संख्या (mol)
- M = मोलरता (mol/L)
- V = घोल का आयतन (लीटर में)
- मोलरता और घोल के आयतन के बीच संबंध (घोल बनाने का उदाहरण): यदि हमें 0.5 M NaCl घोल बनाने के लिए 2 लीटर घोल की आवश्यकता है और हमारे पास 1 M NaCl का घोल है, तो हमें कितना घोल निकालना होगा? M1×V1=M2×V2M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2 1×V1=0.5×21 \times V_1 = 0.5 \times 2 V1=1 लीटरV_1 = 1 \, \text{लीटर} इसका मतलब है कि 1 लीटर 1 M NaCl घोल से 2 लीटर 0.5 M NaCl घोल तैयार किया जा सकता है।
मोलरता के अनुप्रयोग:
- रासायनिक प्रतिक्रियाओं में:
मोलरता का उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संतुलन को स्थापित करने, अभिक्रियाओं की दर मापने और उत्पाद की मात्रा की गणना करने में किया जाता है। - घोल के विश्लेषण में:
प्रयोगशालाओं में मोलरता का उपयोग विभिन्न घोलों की सांद्रता मापने के लिए किया जाता है, जैसे तिर्यक विश्लेषण (titration) में। - इलेक्ट्रोलाइटिक और गैर-इलेक्ट्रोलाइटिक घोलों में:
मोलरता का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट्स (जैसे NaCl) और गैर-इलेक्ट्रोलाइट्स (जैसे ग्लूकोज) की सांद्रता मापने के लिए किया जाता है।
मोलरता और मोलीयल सांद्रता (Molality):
- मोलरता (Molarity): मोल सॉल्यूट/लीटर घोल
- मोलीयल सांद्रता (Molality): मोल सॉल्यूट/किलोग्राम सॉल्वेंट
मोलरता का उपयोग मुख्य रूप से घोल की सांद्रता मापने के लिए किया जाता है, जबकि मोलीयल सांद्रता को तापमान के प्रभाव से बचने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह द्रव की मात्रा के बजाय सॉल्वेंट के द्रव्यमान पर निर्भर होती है।
निष्कर्ष:
मोलरता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो रासायनिक घोलों की सांद्रता मापने के लिए प्रयोग होती है। यह रासायनिक अभिक्रियाओं, घोल निर्माण, और विभिन्न रासायनिक विश्लेषणों में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है।
मोललता (Molality) – महत्वपूर्ण नोट्स
मोललता (Molality) एक सांद्रता की इकाई है जो घोल में सॉल्यूट की मोल संख्या और सॉल्वेंट (घोलक) के द्रव्यमान के आधार पर मापी जाती है। मोललता विशेष रूप से उन मामलों में उपयोगी है जहाँ तापमान में बदलाव होता है, क्योंकि यह सॉल्वेंट के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, जबकि मोलरता (Molarity) घोल के आयतन पर निर्भर करती है, जो तापमान के अनुसार बदल सकता है।
मोललता का परिभाषा:
मोललता (Molality) को m से व्यक्त किया जाता है और इसे निम्नलिखित सूत्र से परिभाषित किया जाता है: Molality (m)=मोल सॉल्यूट (moles of solute)सॉल्वेंट का द्रव्यमान (mass of solvent in kilograms)\text{Molality (m)} = \frac{\text{मोल सॉल्यूट (moles of solute)}}{\text{सॉल्वेंट का द्रव्यमान (mass of solvent in kilograms)}}
यहाँ,
- मोल सॉल्यूट (moles of solute): यह उस पदार्थ की मोल्स की संख्या है जो घोल में घुला हुआ है।
- सॉल्वेंट का द्रव्यमान (mass of solvent): यह उस पदार्थ का द्रव्यमान है जिसमें सॉल्यूट घुला हुआ है, और यह किलोग्राम में मापा जाता है।
मोललता (m) का मात्रक:
मोललता (m) का मात्रक मोल/किलोग्राम (mol/kg) होता है।
मोललता का उदाहरण:
- यदि 1 मोल NaCl को 1 किलोग्राम पानी में घोल लिया जाता है, तो इस घोल की मोललता 1 m (1 मोल प्रति किलोग्राम सॉल्वेंट) होगी।
- यदि 0.5 मोल NaCl को 2 किलोग्राम पानी में घोल लिया जाता है, तो मोललता होगी: m=0.5 मोल2 किलोग्राम=0.25 mm = \frac{0.5 \, \text{मोल}}{2 \, \text{किलोग्राम}} = 0.25 \, \text{m}
मोललता की विशेषताएँ:
- तापमान पर निर्भरता:
- मोललता तापमान पर निर्भर नहीं होती है, क्योंकि यह सॉल्वेंट के द्रव्यमान पर आधारित होती है, जो तापमान परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित रहता है। जबकि मोलरता (Molarity) तापमान के प्रभाव से प्रभावित होती है क्योंकि घोल का आयतन तापमान के साथ बदल सकता है।
- गैसी और द्रव घोलों के लिए उपयोगी:
- मोललता का उपयोग विशेष रूप से उन स्थितियों में किया जाता है जहाँ तापमान में परिवर्तन हो रहा होता है, जैसे घोल में घुलनशीलता (solubility) या तापमान के प्रभाव का अध्ययन करना।
- संसाधनों की माप:
- मोललता का उपयोग अभिक्रियाओं के दौरान रासायनिक और भौतिक गुणों की माप के लिए किया जाता है, जैसे उबालने का बिंदु (boiling point) और ठंडा होने का बिंदु (freezing point)।
मोललता और मोलरता के बीच अंतर:
| विवरण | मोललता (Molality) | मोलरता (Molarity) |
|---|---|---|
| परिभाषा | मोललता सॉल्वेंट के द्रव्यमान (kg) पर आधारित है। | मोलरता घोल के आयतन (L) पर आधारित है। |
| आधार | तापमान परिवर्तन से अप्रभावित है। | तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है। |
| उपयोग | तापमान पर निर्भरता के अध्ययन में प्रयोग होती है। | सामान्य रासायनिक घोलों में प्रयोग होती है। |
| मात्रक | मोल/किलोग्राम (mol/kg) | मोल/लीटर (mol/L) |
मोललता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र:
- सॉल्यूशन के घनत्व और मोललता के बीच संबंध:
- यदि घोल का घनत्व (density) ज्ञात हो और सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट के मोल्स की संख्या ज्ञात हो, तो मोललता की गणना की जा सकती है।
- मोललता और उबालने के बिंदु में वृद्धि (Boiling Point Elevation):
- उबालने के बिंदु में वृद्धि एक महत्त्वपूर्ण भौतिक गुण है जो मोललता के अनुपात में होता है। यह निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है:
- ΔTb\Delta T_b = उबालने के बिंदु में वृद्धि
- KbK_b = उबालने का स्थिरांक (Boiling point elevation constant)
- mm = मोललता
- ii = वॉन होफ कारक (Van’t Hoff factor) जो घुलित पदार्थ के आयनकरण की संख्या को दर्शाता है।
- मोललता और जमने के बिंदु में कमी (Freezing Point Depression):
- मोललता के अनुसार घोल के जमने के बिंदु में कमी होती है, जो निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है:
- ΔTf\Delta T_f = जमने के बिंदु में कमी
- KfK_f = जमने का स्थिरांक (Freezing point depression constant)
- mm = मोललता
- ii = वॉन होफ कारक
मोललता का प्रयोग:
- भौतिक गुणों के अध्ययन में:
- मोललता का उपयोग घोल के उबालने और जमने के बिंदु में वृद्धि/कमी का अध्ययन करने में किया जाता है।
- रासायनिक अभिक्रियाओं में:
- रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और उत्पादों की मात्रा की गणना में मोललता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- आवश्यक घोल तैयार करने में:
- प्रयोगशालाओं में सही मोललता वाले घोल तैयार करने के लिए मोललता का प्रयोग किया जाता है।
मोललता और मोलीयल सांद्रता के बीच अंतर:
| विवरण | मोललता (Molality) | मोलीयल सांद्रता (Molarity) |
|---|---|---|
| संदर्भ | सॉल्वेंट के द्रव्यमान (kg) पर आधारित होता है। | घोल के आयतन (L) पर आधारित होता है। |
| तापमान का प्रभाव | तापमान पर निर्भर नहीं होती। | तापमान के परिवर्तन से प्रभावित होती है। |
| उपयोग | उच्च तापमान वाले प्रयोगों में उपयोगी है। | सामान्य घोलों की सांद्रता मापने के लिए उपयोग होती है। |
निष्कर्ष:
मोललता एक महत्वपूर्ण सांद्रता इकाई है जो विशेष रूप से घोलों में सॉल्यूट की मोल संख्या और सॉल्वेंट के द्रव्यमान के आधार पर घोल की सांद्रता मापने के लिए उपयोग की जाती है। यह तापमान परिवर्तन के प्रभाव से अप्रभावित रहती है और घोल के भौतिक गुणों के अध्ययन, जैसे उबालने के बिंदु और जमने के बिंदु में परिवर्तन, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
मोल प्रभाज (Mole Fraction) या मोल अंश – महत्वपूर्ण नोट्स
मोल प्रभाज (Mole Fraction) किसी मिश्रण में एक घटक के मोलों की संख्या का उस मिश्रण में कुल मोलों की संख्या से अनुपात होता है। इसे मोल अंश (Mole Fraction) भी कहा जाता है। मोल प्रभाज रासायनिक घोलों या मिश्रणों के सांद्रता को व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घोल में प्रत्येक घटक के योगदान को निर्दिष्ट करता है।
मोल प्रभाज का परिभाषा:
मोल प्रभाज (Mole Fraction) एक रासायनिक मिश्रण में किसी घटक के मोलों का कुल मोलों की संख्या से अनुपात होता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जाता है: मोल प्रभाज (X)=किसी घटक के मोल (moles of component)कुल मोलों की संख्या (total moles in mixture)\text{मोल प्रभाज (X)} = \frac{\text{किसी घटक के मोल (moles of component)}}{\text{कुल मोलों की संख्या (total moles in mixture)}}
यहाँ:
- किसी घटक के मोल (moles of component) = उस घटक के मोलों की संख्या।
- कुल मोलों की संख्या (total moles in mixture) = मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का योग।
मोल प्रभाज के प्रकार:
- घटक A का मोल प्रभाज (Xₐ): Xa=nana+nβXₐ = \frac{nₐ}{nₐ + nᵦ} जहाँ:
- nₐ = घटक A के मोल
- nᵦ = घटक B के मोल
- घटक B का मोल प्रभाज (Xᵦ): Xβ=nβna+nβXᵦ = \frac{nᵦ}{nₐ + nᵦ}
मोल प्रभाज का उदाहरण:
- यदि 2 मोल NaCl और 3 मोल H₂O मिलाए जाते हैं, तो मोल प्रभाज निम्नलिखित तरीके से गणना किया जाएगा:
- NaCl का मोल प्रभाज (Xₐ): XNaCl=22+3=25=0.4X_{\text{NaCl}} = \frac{2}{2 + 3} = \frac{2}{5} = 0.4
- H₂O का मोल प्रभाज (Xᵦ): XH₂O=32+3=35=0.6X_{\text{H₂O}} = \frac{3}{2 + 3} = \frac{3}{5} = 0.6
मोल प्रभाज के लाभ:
- सार्वभौमिकता:
मोल प्रभाज किसी भी परिस्थिति में उपयोगी हो सकता है क्योंकि यह मोलों पर आधारित होता है, जो तापमान या दबाव के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। इसका मतलब है कि यह सांद्रता की एक स्थिर इकाई है। - रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोग:
रासायनिक अभिक्रियाओं में मोल प्रभाज का उपयोग विभिन्न घटकों के बीच अभिक्रिया की संभावना और उत्पन्न होने वाले उत्पादों के अनुपात का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। - विश्लेषणात्मक रसायन में उपयोग:
मोल प्रभाज का उपयोग घोलों की पिचाई, वाष्प दाब, उबालने के बिंदु में वृद्धि, और जमने के बिंदु में कमी जैसे भौतिक गुणों के अध्ययन में किया जाता है।
मोल प्रभाज और मोलरता में अंतर:
| विवरण | मोल प्रभाज (Mole Fraction) | मोलरता (Molarity) |
|---|---|---|
| संदर्भ | किसी घटक के मोलों का अनुपात होता है। | घोल के आयतन के अनुसार सांद्रता होती है। |
| मात्रक | बिना इकाई (Unitless) होता है। | मोल/लीटर (mol/L) के रूप में व्यक्त होता है। |
| तापमान पर प्रभाव | तापमान पर निर्भर नहीं होता है। | तापमान के प्रभाव से प्रभावित होता है। |
| प्रयोग | मिश्रण में विभिन्न घटकों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है। | घोल की सांद्रता मापने के लिए उपयोग होता है। |
मोल प्रभाज का प्रयोग:
- सांद्रता के अध्ययन में:
मोल प्रभाज का उपयोग घोलों की सांद्रता मापने के लिए किया जाता है। यह भौतिक गुणों जैसे वाष्प दाब, जमने के बिंदु और उबालने के बिंदु में कमी या वृद्धि के अध्ययन में काम आता है। - गैस के व्यवहार का अध्ययन:
मोल प्रभाज का उपयोग गैसों के मिश्रण में उनके व्यावहारिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। गैसों के मिश्रण में मोल प्रभाज के आधार पर उनकी कुल दबाव का अनुमान लगाया जा सकता है (आधारित राउल्ट्स नियम पर)। - रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन:
मोल प्रभाज का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन को निर्धारित करने और रिएक्शन की गति को समझने में किया जाता है। - संगति और विलयन गुण:
मोल प्रभाज का उपयोग मिश्रणों की संगति और घोल के विभिन्न गुणों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जैसे वाष्प दाब में कमी, उबालने का बिंदु, ठंडा होने का बिंदु आदि।
मोल प्रभाज और अन्य सांद्रता इकाइयाँ (जैसे मोलीयल सांद्रता) में अंतर:
- मोल प्रभाज (Mole Fraction): यह बिना इकाई के होता है और किसी घटक के मोलों की संख्या का अनुपात है। यह घोल में घुलने वाले सभी घटकों के मोलों के अनुपात के रूप में व्यक्त होता है।
- मोलीयल सांद्रता (Molality): यह घोल में सॉल्वेंट के द्रव्यमान (किलोग्राम) और सॉल्यूट के मोलों के अनुपात के रूप में मापी जाती है। यह तापमान के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है।
मोल प्रभाज का गणना उदाहरण:
- घटक A और B के मोल प्रभाज की गणना: मान लीजिए 2 मोल A और 3 मोल B मिलाए गए हैं।
- कुल मोल = 2 (A) + 3 (B) = 5 मोल।
- A का मोल प्रभाज (Xₐ): Xa=25=0.4Xₐ = \frac{2}{5} = 0.4
- B का मोल प्रभाज (Xᵦ): Xβ=35=0.6Xᵦ = \frac{3}{5} = 0.6
निष्कर्ष:
मोल प्रभाज (Mole Fraction) एक महत्वपूर्ण सांद्रता की इकाई है जिसका उपयोग विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं, मिश्रणों के गुण, और भौतिक गुणों के अध्ययन में किया जाता है। यह मोलों के अनुपात पर आधारित होता है और तापमान पर निर्भर नहीं होता है, जिससे यह मोलरता (Molarity) जैसे अन्य सांद्रता उपायों से अलग होता है। मोल प्रभाज का उपयोग विभिन्न रासायनिक और भौतिक विश्लेषणों में किया जाता है, और यह एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है रसायनशास्त्र और भौतिक रसायन में।